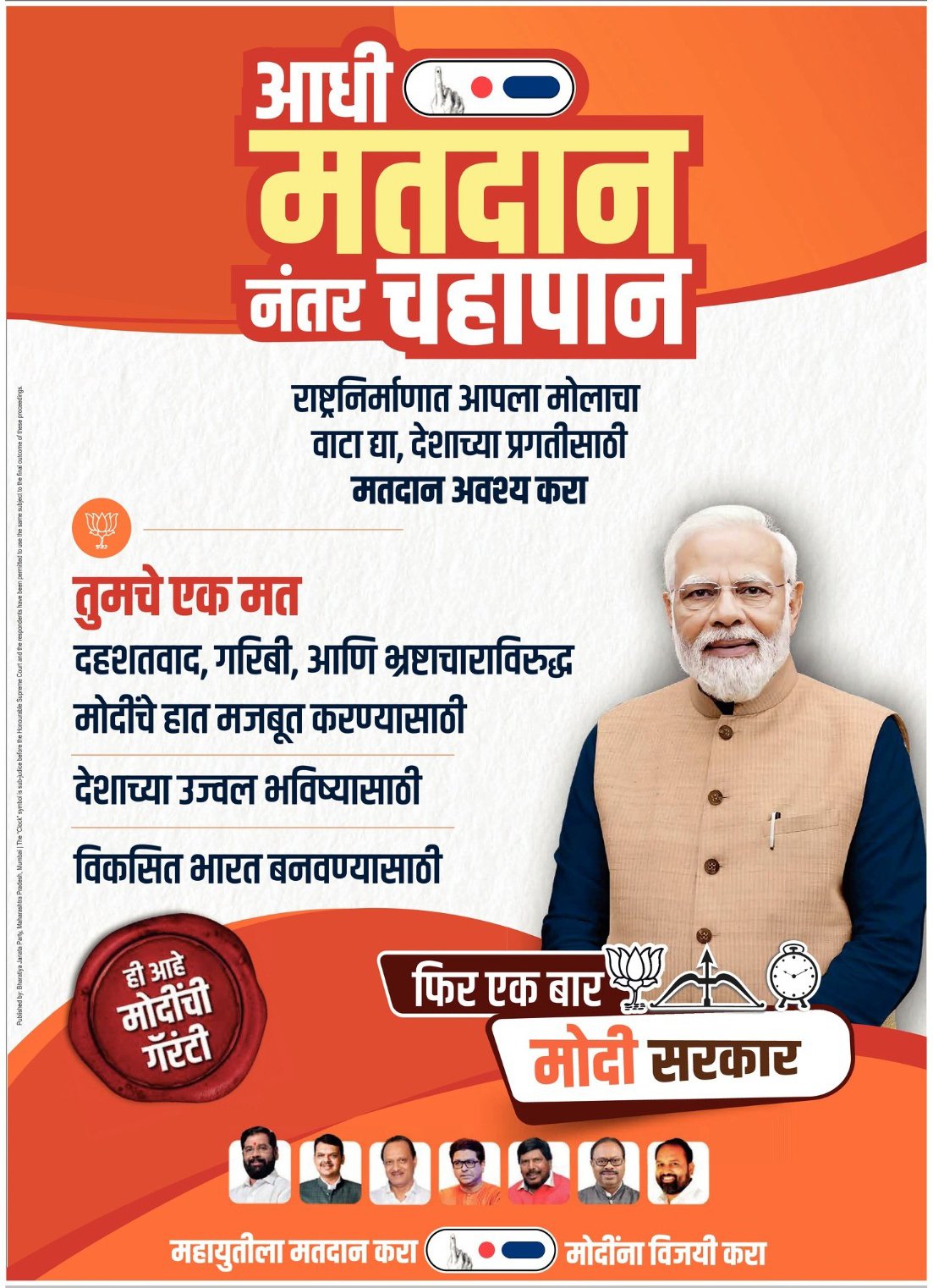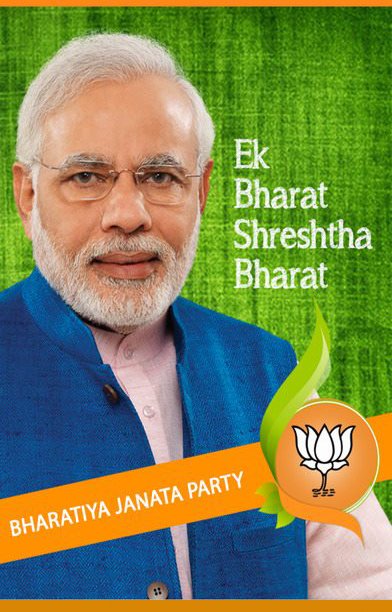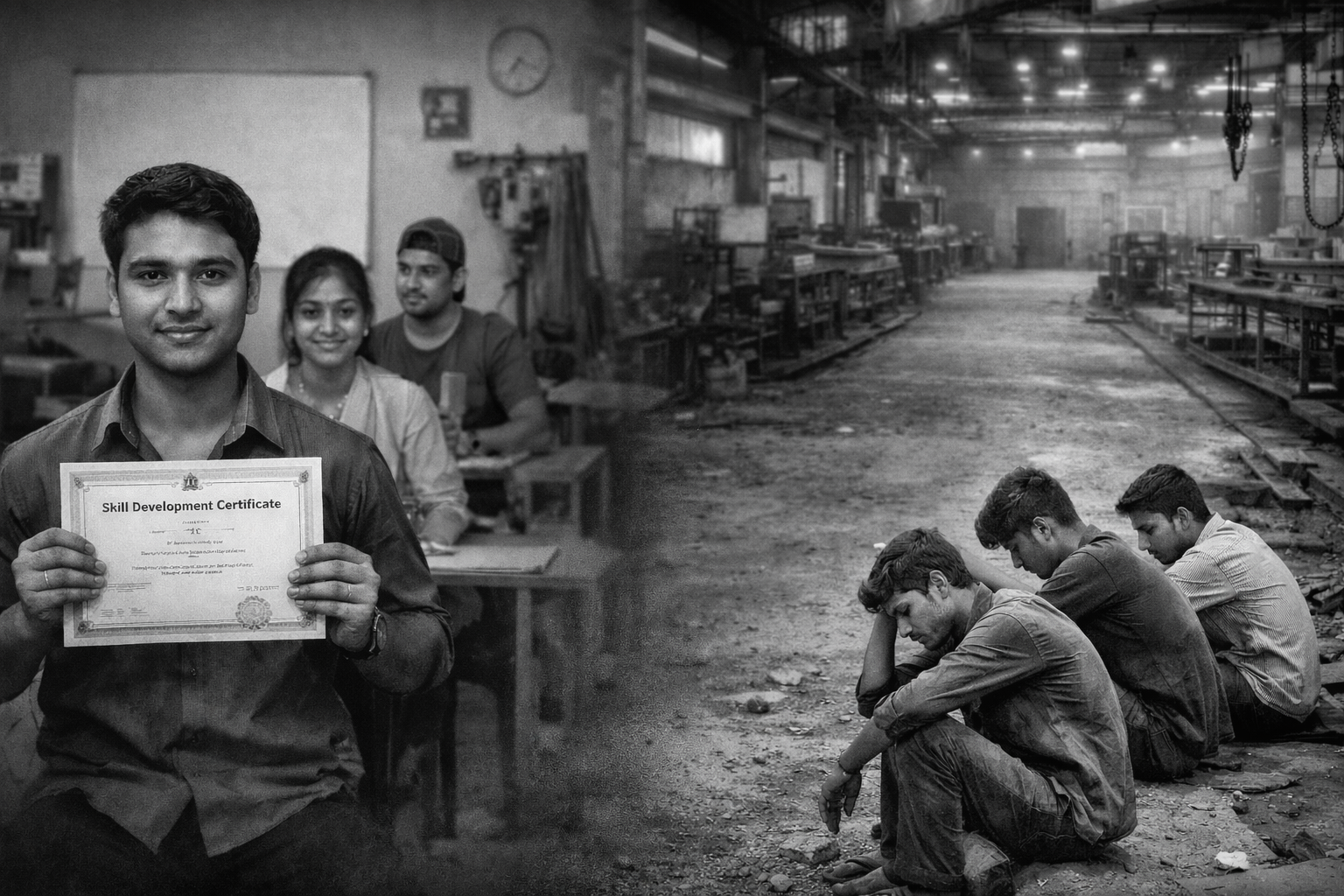नई दिल्ली/अहमदाबाद, 26फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को एक अहम फैसला सुनाते हुए अमेरिका में रह रहे एक व्यक्ति के प्रत्यर्पण से जुड़े निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। यह आदेश घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत दायर एक मामले में पारित किया गया था, जिसमें पत्नी ने अपने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। निचली अदालत ने आरोपी की गैर-मौजूदगी को आधार बनाते हुए प्रत्यर्पण का आदेश दिया था, जिसे पति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
देश की शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा मामलों की प्रकृति अर्ध-आपराधिक (semi-criminal) होती है, और ऐसे मामलों में आरोपी की न्यायालय में प्रत्यक्ष उपस्थिति आवश्यक नहीं है। चूंकि आरोपी अमेरिका में रह रहा था और निचली अदालत में पेश नहीं हो सकता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को कानूनी रूप से असंगत मानते हुए निरस्त कर दिया।
Live Law की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा, “हम देख सकते हैं कि चूंकि DV Act के तहत कार्यवाही अर्ध-आपराधिक प्रकृति की है, इसलिए इन कार्यवाहियों में अपीलकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।”
प्रत्यर्पण क्या है और यह कैसे काम करता है?
प्रत्यर्पण एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से एक देश किसी व्यक्ति को दूसरे देश को सौंपता है, ताकि उस व्यक्ति पर वहां के कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जा सके या सजा दी जा सके। यह प्रक्रिया दो देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि पर आधारित होती है, जिसमें दोनों देश आपसी सहमति से अपराधियों के आदान-प्रदान के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करते हैं।
प्रत्यर्पण प्रक्रिया के मुख्य चरण:
- प्रत्यर्पण अनुरोध: जिस देश में अपराध हुआ है, वह दूसरे देश से आरोपी को सौंपने का अनुरोध करता है।
- कानूनी समीक्षा: अनुरोध प्राप्त करने वाला देश अपने कानूनों और संधि की शर्तों के आधार पर अनुरोध की समीक्षा करता है।
- न्यायिक सुनवाई: आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाता है, जहां प्रत्यर्पण की वैधता पर निर्णय लिया जाता है।
- अंतिम निर्णय: न्यायिक प्रक्रिया के बाद, संबंधित प्राधिकरण प्रत्यर्पण को मंजूरी देते हैं या अस्वीकार करते हैं।
प्रत्यर्पण प्रक्रिया में कई कानूनी, राजनीतिक और कूटनीतिक पहलू शामिल होते हैं, जो इसे जटिल बनाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ मामलों में मानवाधिकारों का संरक्षण, दोहरे अपराध (double jeopardy) का सिद्धांत, और राजनीतिक अपराधों के लिए प्रत्यर्पण न करना जैसी शर्तें लागू हो सकती हैं।
भारत में, प्रत्यर्पण से संबंधित प्रावधान ‘प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962’ में विस्तृत हैं।अधिक जानकारी के लिए, आप विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध प्रत्यर्पण से संबंधित सामान्य प्रश्न पृष्ठ भी देख सकते हैं।
प्रमुख चर्चित मामले: अबू सलेम, नीरव मोदी, विजय माल्या और तहव्वुर राणा
 फोटो: साभार ABP News
फोटो: साभार ABP News
अबू सलेम: 1993 के मुंबई बम धमाकों के मुख्य आरोपियों में से एक, अबू सलेम को 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था। यह प्रक्रिया कई कानूनी और कूटनीतिक चुनौतियों के बाद सफल हुई।
 फोटो: साभार बिजनेस स्टैंडर्ड
फोटो: साभार बिजनेस स्टैंडर्ड
नीरव मोदी: पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी को भारत लाने के लिए ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। ब्रिटिश अदालत ने प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है, लेकिन नीरव मोदी ने इसके खिलाफ उच्च अदालत में अपील की थी।अधिक जानकारी के लिए, आप Dainik Bhaskar की संबंधित रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं।
 फोटो: साभार नवभारत टाइम्स
फोटो: साभार नवभारत टाइम्स
विजय माल्या: वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का सामना कर रहे विजय माल्या भी ब्रिटेन में हैं। उनके प्रत्यर्पण के लिए भारतीय सरकार ने ब्रिटिश अधिकारियों से अनुरोध किया है, और कानूनी प्रक्रिया जारी है। जी बिज़नेस के अनुसार इस सप्ताह लंदन के हाईकोर्ट में माल्या के दिवाला आदेश से संबंधित तीन परस्पर जुड़ी अपीलों की सुनवाई पूरी हो गई.।
 फोटो: साभार ABP Live
फोटो: साभार ABP Live
तहव्वुर राणा: 26/11 मुंबई हमलों के मामले में आरोपी तहव्वुर राणा का मामला भी महत्वपूर्ण है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी 2025 को राणा की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिससे भारत में उसका प्रत्यर्पण संभव हो सका। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार तहव्वुर राणा को जल्द भारत लाया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला और चर्चित प्रत्यर्पण मामलों का कनेक्शन
- सुप्रीम कोर्ट का यह ताज़ा फैसला भारतीय न्यायिक प्रणाली में एक नई मिसाल स्थापित करता है।
- यह निर्णय न केवल कानूनी प्रक्रियाओं की व्याख्या को स्पष्ट करता है, बल्कि न्याय की अवधारणा में मानवीय दृष्टिकोण को भी मजबूती से स्थापित करता है।
- इससे प्रत्यर्पण प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता को नया आधार मिलेगा, जो भविष्य में समान मामलों के निपटारे में मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करेगा।
इस कनेक्शन की विस्तृत और सरल व्याख्या
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय न्याय व्यवस्था अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करते हुए निष्पक्ष सुनवाई प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह उन प्रत्यर्पण मामलों को भी प्रभावित कर सकता है, जिनमें आरोपी यह दावा करते हैं कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी।
इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारतीय न्यायपालिका को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक मजबूत और विश्वसनीय साबित कर सकता है, जिससे भारत के प्रत्यर्पण अनुरोधों की स्वीकार्यता में वृद्धि हो सकती है।
इसके अलावा, यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि आरोपी की गैर-मौजूदगी में भी न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से संचालित की जा सकती है। इससे भविष्य में अभियुक्तों द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति न होने के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की संभावनाएं कम होंगी, और प्रत्यर्पण प्रक्रिया में भी इसे एक मिसाल के रूप में देखा जाएगा।
यह फैसला यह भी सुनिश्चित करता है कि अदालतें अभियुक्तों की अनुपस्थिति में भी न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला सकती हैं, बशर्ते यह निष्पक्षता के सभी मानकों को पूरा करता हो। इससे प्रत्यर्पण संबंधी मामलों में न्यायिक प्रणाली अधिक प्रभावी और विश्वसनीय साबित होगी।
एक नई कानूनी मिसाल
सुप्रीम कोर्ट का यह ताज़ा फैसला भारतीय न्यायिक प्रणाली में एक नई मिसाल स्थापित करता है। यह निर्णय न केवल कानूनी प्रक्रियाओं की व्याख्या को स्पष्ट करता है, बल्कि न्याय की अवधारणा में मानवीय दृष्टिकोण को भी मजबूती से स्थापित करता है।
इससे प्रत्यर्पण प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता को नया आधार मिलेगा, जो भविष्य में समान मामलों के निपटारे में मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करेगा।