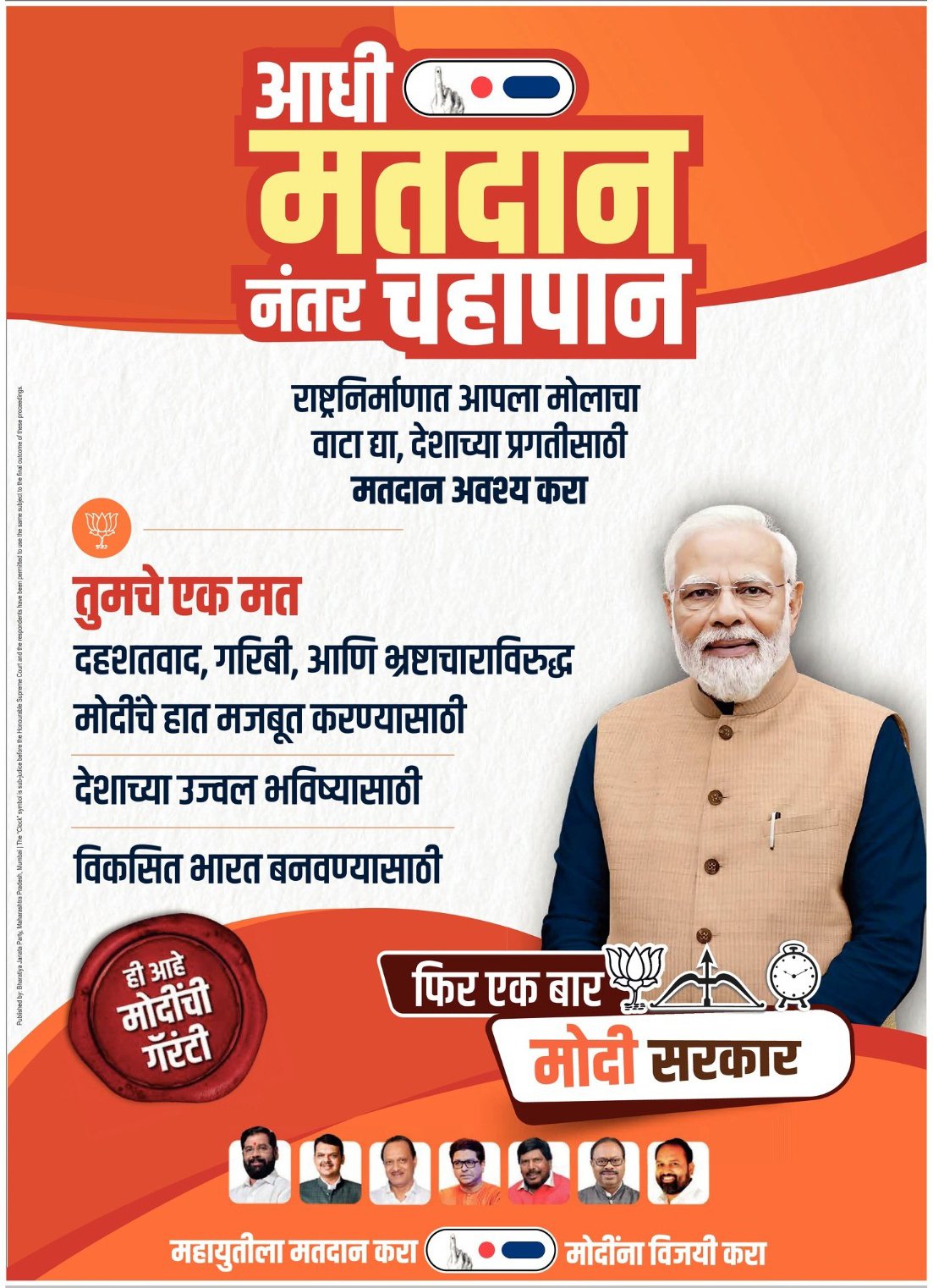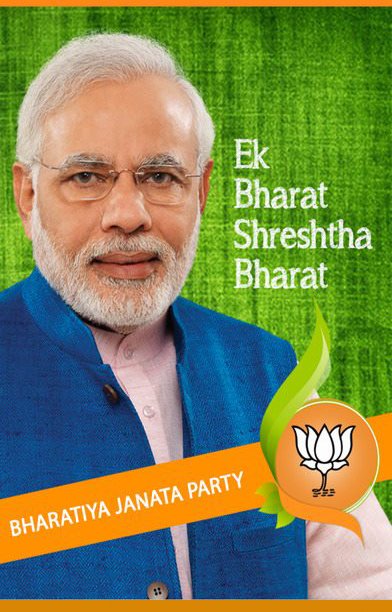अहमदाबाद, 9 जनवरी 2026। न्याय की सबसे कठिन परीक्षा यह नहीं होती कि वह किस मामले में क्या फैसला देता है। असली परीक्षा यह होती है कि क्या वह समान परिस्थितियों में स्वयं को समान रूप से दोहराता है। जब यही निरंतरता टूटती दिखाई देती है, तब सवाल किसी एक आरोपी, एक आदेश या एक पीठ तक सीमित नहीं रहता। सवाल न्याय की प्रक्रिया और उसकी विश्वसनीयता पर टिक जाता है।
हाल के वर्षों में जमानत से जुड़े कुछ न्यायिक आदेशों ने ठीक यही स्थिति पैदा की है। एक ओर अदालतें यह स्वीकार करती दिखाई देती हैं कि लंबी न्यायिक हिरासत और मुकदमे की देरी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्षीण करती है। दूसरी ओर, उन्हीं परिस्थितियों में अदालतें यह भी कहती हैं कि समय यानी देरी अपने आप में जमानत का आधार नहीं हो सकता। यही विरोधाभास आज आम पाठक, वकील और न्याय में भरोसा रखने वाले नागरिक के भीतर असमंजस पैदा कर रहा है।
इसी संदर्भ में उमर ख़ालिद और शरजील इमाम का मामला सामने आता है। दोनों पर UAPA (गैरकानूनी गतिविधियाँ निवारण अधिनियम, 1967) के तहत गंभीर आरोप हैं और वे पाँच वर्ष से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं। ट्रायल अभी अंतिम चरण से दूर है।
5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएँ खारिज करते हुए यह माना कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत होते हैं जिन्हें इस चरण पर पूरी तरह अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उनकी कथित भूमिका अन्य सह-आरोपियों से भिन्न मानी गई है और इसलिए उन्हें समान आधार पर नहीं रखा जा सकता।
UAPA की धारा 43D(5) के तहत, जमानत पर विचार करते समय शीर्ष अदालत इस प्रारंभिक चरण में आरोपों की गहन या सूक्ष्म पड़ताल नहीं करती। वह केवल यह देखती है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सामग्री पूरी तरह निराधार या असंभव तो नहीं है। इसी वैधानिक सीमा के भीतर जमानत से इनकार किया गया।
अदालत ने यह भी दर्ज किया कि लंबी न्यायिक हिरासत अपने आप में एक महत्वपूर्ण कारक अवश्य है, किंतु इस स्तर पर वह ऐसी संवैधानिक स्थिति तक नहीं पहुँची है, जहाँ केवल समय के आधार पर UAPA की वैधानिक बाधा को दरकिनार किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, अभियोजन सामग्री की प्रकृति, आरोपों की जटिलता और मुकदमे की वर्तमान अवस्था को देखते हुए निरंतर हिरासत को इस चरण पर संविधान के प्रतिकूल नहीं माना जा सकता।
हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निष्कर्ष अंतिम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद, अथवा आदेश की तारीख से एक वर्ष पूरा होने पर, जो भी पहले हो, उमर ख़ालिद और शरजील इमाम पुनः जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रश्न को अदालत ने एक निरंतर न्यायिक परीक्षण के रूप में खुला रखा।
शीर्ष अदालत ने आगे यह रेखांकित किया कि यदि संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने अथवा आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात पुनः जमानत याचिका दायर की जाती है, तो उस याचिका पर उस समय मुकदमे की वास्तविक प्रगति और परिस्थितियों के आधार पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाएगा।
अदालत ने यह विशेष रूप से स्पष्ट किया कि भविष्य में इस प्रकार की किसी भी जमानत याचिका पर विचार करते समय न तो वर्तमान आदेश और न ही पूर्ववर्ती आदेश किसी प्रकार से निर्णायक प्रभाव डालेंगे।
महत्वपूर्ण यह भी है कि इसी आदेश में शीर्ष अदालत ने अन्य पाँच आरोपियों (गुलफिशा फ़ातिमा, मीरान हैदर, शिफ़ा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम ख़ान और शादाब अहमद) को जमानत प्रदान की। इन मामलों में शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया कि जमानत देना आरोपों की गंभीरता को कम करना या दोष पर कोई राय देना नहीं है, बल्कि यह न्यायिक विवेक का संतुलित प्रयोग है। जमानत के साथ कड़ी शर्तें भी लगाई गईं।
जमानत को अदालत ने अत्यंत कड़े सुरक्षा-उपबंधों से जोड़ा। आरोपियों को प्रत्येक सप्ताह सोमवार और गुरुवार को प्रातः 10 से 12 बजे के बीच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, पुलिस मुख्यालय, जय सिंह मार्ग, नई दिल्ली स्थित थाना प्रभारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया गया। थाना प्रभारी को प्रत्येक आरोपी के लिए अलग उपस्थिति रजिस्टर बनाए रखने और उसकी मासिक अनुपालन रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट को प्रेषित करने का आदेश दिया गया।
इन पाँच मामलों में अदालत ने यह संतुलित निष्कर्ष निकाला कि इस चरण पर निरंतर कारावास निष्पक्ष मुकदमे के लिए अपरिहार्य प्रतीत नहीं होता, बशर्ते जमानत को कड़े और प्रभावी सुरक्षा-उपबंधों से बाँधा जाए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह राहत न तो आरोपों की गंभीरता को कम करती है और न ही किसी प्रकार की दोष-मुक्ति का संकेत देती है, बल्कि यह संविधान के दायरे में किया गया एक संतुलित और नियंत्रित न्यायिक विवेक है।
यह भेद इस तथ्य को रेखांकित करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी सामूहिक या यांत्रिक दृष्टिकोण को नहीं अपनाया, बल्कि प्रत्येक आरोपी की भूमिका, उपलब्ध सामग्री और वैधानिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग निष्कर्ष निकाले।
कानून की दृष्टि से यह तर्क अपने आप में असंगत नहीं है। लेकिन यहीं से वह प्रश्न उभरता है, जो केवल इस एक मामले तक सीमित नहीं रहता। क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट, इसी कठोर कानून के संदर्भ में, पूर्व में एक अलग और अधिक संतुलित दृष्टिकोण भी अपना चुका है।
के. ए. नजीब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में यह सिद्धांत स्थापित किया था कि कोई भी विशेष या कठोर कानून संविधान के अनुच्छेद 21 के संरक्षण को निष्क्रिय नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि ट्रायल के निकट भविष्य में पूर्ण होने की वास्तविक संभावना नहीं दिखती और कोई व्यक्ति लंबे समय तक विचाराधीन हिरासत में बना रहता है, तो उसे अनिश्चितकाल तक जेल में रखना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।
इसी संवैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर जमानत प्रदान की गई थी। यह निर्णय न तो कभी पलटा गया है और न ही अप्रासंगिक ठहराया गया है; वह आज भी भारतीय न्यायशास्त्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित न्याय के अधिकार से जुड़ा एक जीवित और मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है।
यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि के. ए. नजीब का मामला और उमर ख़ालिद–शरजील इमाम का मामला, दोनों ही एक ही कानून (गैरकानूनी गतिविधियाँ निवारण अधिनियम, 1967) के अंतर्गत हैं और दोनों में जमानत पर विचार करते समय वही वैधानिक कसौटी, UAPA की धारा 43D(5), लागू होती है। अंतर कानून का नहीं, बल्कि उस कसौटी के न्यायिक प्रयोग का है—जहाँ एक मामले में अनुच्छेद 21 के आधार पर उसकी कठोरता शिथिल की गई, वहीं दूसरे में उसे इस चरण पर प्रभावी माना गया।
जब समय एक-सा नहीं रहता
इसी बिंदु पर न्याय की कसौटी पर पहला बड़ा प्रश्न उभरता है—जब वही अदालत, वही संविधान और वही अनुच्छेद 21 मौजूद हैं, तो समय को एक मामले में मानवीय आधार और दूसरे में अप्रासंगिक तथ्य कैसे माना जा सकता है।
यह प्रश्न तब और गहराता है, जब दोषसिद्ध मामलों की ओर दृष्टि जाती है। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे गंभीर अपराध में दोषसिद्ध व्यक्ति को यह कहते हुए अंतरिम राहत दी गई कि अपील के अंतिम निस्तारण में समय लगेगा और तब तक जेल में रखना उचित नहीं होगा। यहाँ समय एक मानवीय तर्क बन जाता है। यह तर्क अपने आप में असंवैधानिक नहीं है। लेकिन यही तर्क जब विचाराधीन कैदियों के लिए अनुपलब्ध हो जाता है, तो न्याय की समानता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।
हालाँकि, यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त अंतरिम राहत के आदेश के क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। यह तथ्य अपने आप में उस न्यायिक तर्क को निष्प्रभावी नहीं करता, बल्कि यह दर्शाता है कि समय को मानवीय आधार मानने की प्रवृत्ति न्यायिक विमर्श का हिस्सा बनी हुई है, भले ही उसका अंतिम प्रभाव अभी लंबित हो।
भारतीय न्यायशास्त्र लंबे समय से इस मूल सिद्धांत को स्वीकार करता आया है कि दोषसिद्धि से पहले कारावास दंड का विकल्प नहीं हो सकता। जमानत का अर्थ अपराध को माफ करना नहीं है; उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विचाराधीन हिरासत सजा का रूप न ले।
यह सिद्धांत नया नहीं है। गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जमानत देते समय न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग दंडात्मक दृष्टि से नहीं, बल्कि इस उद्देश्य से किया जाना चाहिए कि आरोपी मुकदमे के दौरान न्यायिक प्रक्रिया के समक्ष उपस्थित रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यह रेखांकित किया था कि जमानत सजा का विकल्प नहीं है और न ही उसे दंड के रूप में देखा जाना चाहिए। यह कोई भावनात्मक उदारता नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा में न्याय का अनुशासन है।
संजय चंद्रा बनाम सीबीआई (2011) में सुप्रीम कोर्ट ने इस विचार को सबसे स्पष्ट शब्दों में रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमानत का उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न ही निवारक। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि सजा दोषसिद्धि के बाद शुरू होती है; यह भी समझना आवश्यक है कि दोषसिद्धि से पहले कारावास में अपने आप में एक महत्वपूर्ण दंडात्मक तत्व मौजूद होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह भी कहा था कि किसी गैर-दोषसिद्ध व्यक्ति को “सबक सिखाने” के उद्देश्य से जेल में रखना न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। जमानत का मूल उद्देश्य यही है कि आरोपी स्वतंत्र रहते हुए मुकदमे में उपस्थित रहे, ताकि दोषसिद्धि से पहले जेल, सजा का रूप न ले।
भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर यह भी स्पष्ट किया है कि न्याय का मूल सूत्र “जमानत नियम है और जेल अपवाद” ही होना चाहिए। व्यक्तिगत आज़ादी की इसी मशाल को और रोशन करते हुए अर्नब गोस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक टिप्पणी की थी कि “व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रक्रिया की वेदी पर बलि नहीं चढ़ाया जा सकता।”
शीर्ष अदालत का यह रुख गंभीर आर्थिक अपराधों में भी अडिग रहा है। पी. चिदंबरम के मामले में कोर्ट ने माना कि महज़ आरोपों की गंभीरता के आधार पर किसी को अनिश्चितकाल तक कैद रखना न्याय का विकल्प नहीं हो सकता। यहाँ भी समय और स्वतंत्रता को न्यायिक विवेक के केंद्र में रखा गया।
इन सभी निर्णयों में एक साझा तत्व उभरता है—समय। यही वह बिंदु है, जहाँ अदालत का तर्क आम नागरिक के अनुभव से टकराता हुआ दिखाई देता है। कभी वही समय मानवीय आधार बन जाता है, तो कभी वही समय जमानत के लिए अपर्याप्त ठहरा दिया जाता है। यही चयनात्मकता आम नागरिक को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मौलिक अधिकार परिस्थितियों के अनुसार स्थगित किए जा सकते हैं।
यह कहना आसान होगा कि UAPA एक विशेष कानून है और उसमें सामान्य जमानत सिद्धांत लागू नहीं होते। यह तर्क कानूनी रूप से सही हो सकता है। लेकिन यह उत्तर अधूरा रह जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्वयं यह मान चुका है कि कोई भी विशेष कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। यहीं से यह बहस किसी एक आरोपी की पहचान से आगे बढ़कर न्याय की उस आत्मा पर केंद्रित हो जाती है, जो समान परिस्थितियों में समान कसौटी की अपेक्षा करती है।
5 जनवरी 2026 को दिए गए आदेश के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह भी निर्देश दिया कि मुकदमे की कार्यवाही को यथाशीघ्र आगे बढ़ाया जाए, विशेष रूप से संरक्षित गवाहों की गवाही में अनावश्यक विलंब न हो। सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन और बचाव, दोनों से अपेक्षा की कि वे टालने योग्य स्थगनों से बचें, ताकि मुकदमे की प्रगति समयबद्ध और निष्पक्ष बनी रहे।
यह लेख किसी व्यक्ति को निर्दोष या दोषी घोषित करने का प्रयास नहीं करता। यह लेख अदालत के अधिकार क्षेत्र पर प्रश्न नहीं उठाता। केवल यह दर्ज करता है कि जब समान परिस्थितियों में न्यायिक तर्क अलग-अलग दिखाई देने लगें, तो भरोसा कमजोर पड़ने लगता है।
लोकतंत्र में न्याय का सही होना निस्संदेह आवश्यक है। लेकिन उतना ही आवश्यक यह भी है कि वह समान दिखे। शायद आज न्याय की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह कठिन और असहज मामलों में भी स्वयं को एक-सा बनाए रख सके, ताकि विश्वास किसी एक निर्णय पर नहीं, बल्कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया की निरंतरता पर टिका रह सके।