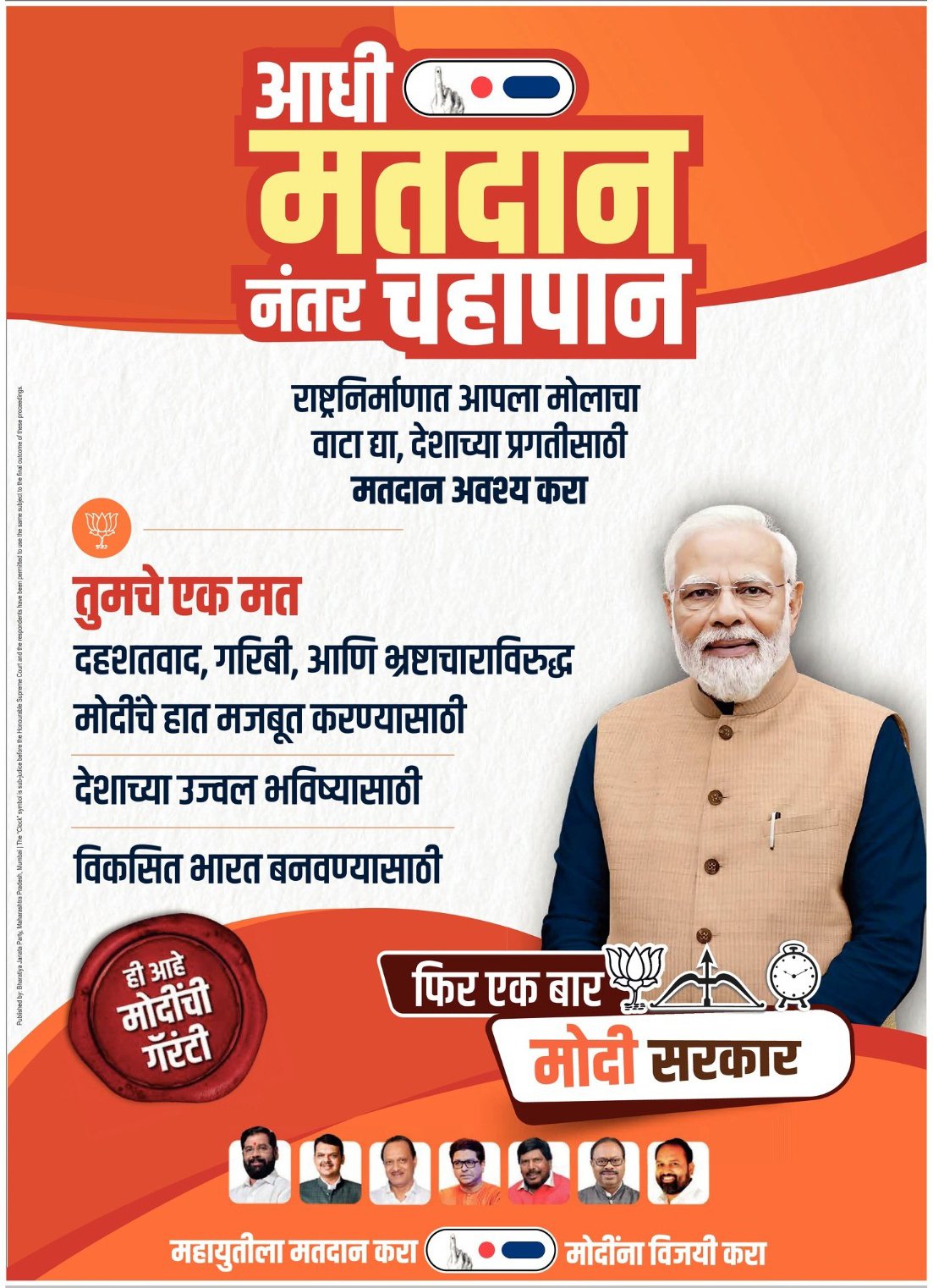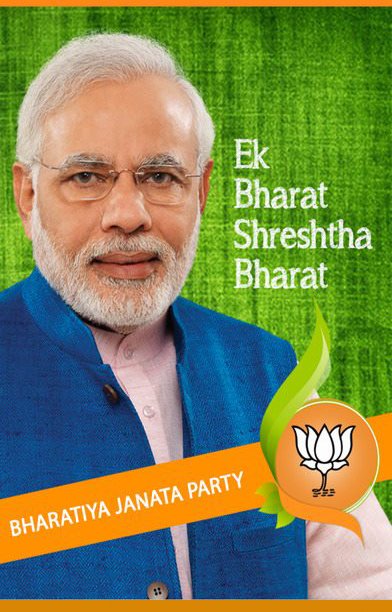कानून के दायरे में आया फैसला, समाज के कटघरे में खड़ा न्याय…
दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को एक ऐसा आदेश पारित किया, जिसने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया कि जब न्याय की प्रक्रिया लंबी हो जाती है, तो उसके हर पड़ाव को समाज किस दृष्टि से देखता है। अदालत का यह आदेश उन्नाव में नाबालिग से जुड़े यौन अपराध के एक अत्यंत गंभीर और चर्चित मामले से संबंधित है।
इस आदेश के तहत दोषसिद्ध पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आपराधिक अपील लंबित रहने तक सजा के क्रियान्वयन को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया। यही वह मामला है जिसमें निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषसिद्धि करते हुए शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
हालांकि यह स्पष्ट किया गया कि यह आदेश दोषसिद्धि पर अंतिम निर्णय नहीं है और केवल सजा निलंबन से जुड़ा एक अंतरिम न्यायिक आदेश है, फिर भी इसके सामने आते ही देश के विभिन्न हिस्सों में तीखी प्रतिक्रियाएँ देखने को मिलीं।
उल्लेखनीय है कि इस आदेश के बावजूद सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सके, क्योंकि वे पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत से जुड़े एक अन्य मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-II) के तहत दोषसिद्ध होकर अलग से दस वर्ष की सजा काट रहे हैं।
इसके पश्चात 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश के संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी और कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि यह विवाद अब केवल उच्च न्यायालय के स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निर्णायक न्यायिक विमर्श के चरण में प्रवेश कर चुका है।
मामला क्या था
यह आपराधिक मामला 4 जून 2017 की एक घटना से जुड़ा है, जिसमें आरोप था कि एक नाबालिग लड़की को नौकरी का झांसा देकर आरोपी के निवास पर ले जाया गया और उसके साथ बलात्कार किया गया।
बाद में इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपी गई। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यह वही मामला है, जिसमें पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत, कथित पुलिस निष्क्रियता और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इसी कारण यह प्रकरण केवल एक आपराधिक मुकदमे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय संवेदनशीलता का विषय बन गया।
अदालत के बाहर विरोध, अदालत के भीतर कानूनी बहस

हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली हाईकोर्ट परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। पीड़िता के परिवार से जुड़े लोग, महिला एवं बाल अधिकारों से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों की प्रतिनिधि महिलाएँ और सामाजिक कार्यकर्ता अदालत के बाहर एकत्र हुए और सजा निलंबन के फैसले पर आपत्ति जताई। इन प्रदर्शनों में यह स्वर प्रमुख रहा कि इस आदेश से पीड़ित पक्ष को न्याय मिलता हुआ प्रतीत नहीं होता।
यह विरोध अदालत के कामकाज के खिलाफ नहीं, बल्कि उस असंतोष की अभिव्यक्ति था जो इस मामले से समाज के एक बड़े हिस्से में लंबे समय से मौजूद है। यह प्रतिक्रिया न्यायिक आदेश के कानूनी औचित्य से अधिक उसके सामाजिक प्रभाव से जुड़ी हुई दिखाई देती है।
अदालत ने क्या कहा, और क्या नहीं कहा
दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश न तो यह कहता है कि अपराध नहीं हुआ, और न ही यह कि निचली अदालत का फैसला गलत था। उच्च अदालत ने स्पष्ट किया है कि दोषसिद्धि पर अंतिम निर्णय अभी शेष है।
हाईकोर्ट का यह आदेश केवल इस सीमित प्रश्न से जुड़ा है कि जब किसी व्यक्ति की आपराधिक अपील उच्च न्यायालय में लंबित हो और उसके शीघ्र निपटारे की संभावना न हो, तब क्या सजा को अंतिम निर्णय तक प्रभावी रखा जाना चाहिए या नहीं।
उच्च अदालत ने विशेष रूप से यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश में किए गए सभी निष्कर्ष केवल प्रथम दृष्टया (prima facie) हैं। इन निष्कर्षों को अपील की अंतिम सुनवाई में साक्ष्य और मेरिट के आधार पर पुनः परखा जाएगा। अर्थात, यह आदेश न तो दोषमुक्ति की घोषणा करता है और न ही अपील के अंतिम परिणाम का कोई संकेत देता है।
POCSO कानून और ‘Public Servant’ की व्याख्या
इस आदेश का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद पहलू पॉक्सो कानून की एक कानूनी व्याख्या से जुड़ा है। निचली अदालत ने आरोपी को उस धारा के तहत दोषी माना था, जो तब लागू होती है जब अपराध किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया गया हो। चूंकि आरोपी उस समय विधायक था, इसलिए उसे पब्लिक सर्वेंट मानते हुए पॉक्सो की सबसे कठोर धारा लागू की गई थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम स्वयं ’पब्लिक सर्वेंट’ की कोई स्वतंत्र परिभाषा नहीं देता। कानून यह निर्देश देता है कि ऐसे शब्दों का अर्थ भारतीय दंड संहिता (IPC) से लिया जाएगा। भारतीय दंड संहिता में विधायक को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया है और इस विषय पर एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट का पूर्व निर्णय भी मौजूद है।
उच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि यह निष्कर्ष केवल सजा निलंबन के प्रश्न तक सीमित है। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि IPC की वैकल्पिक कठोर धाराएँ 376(2)(f)/(k) जोड़ने का प्रयास ट्रायल स्तर पर ही 20 अगस्त 2019 को खारिज हो चुका था, और उसे न तो पीड़िता पक्ष ने चुनौती दी और न ही CBI ने समर्थन किया।
इसलिए सजा निलंबन के इस चरण पर उन धाराओं के आधार पर कठोरतम दंड की संभावना खड़ी करके राहत रोकी नहीं जा सकती। यह न तो अपील के अंतिम परिणाम का संकेत है और न ही दोषसिद्धि पर कोई अंतिम टिप्पणी।
समय, सजा और संविधान का सवाल
हाईकोर्ट ने इस आदेश में समय के पहलू को एक महत्वपूर्ण कारक माना। उच्च अदालत ने दर्ज किया कि आरोपी सात वर्ष से अधिक समय तक जेल में रह चुका है, जबकि घटना के समय लागू कानून में न्यूनतम सजा सात वर्ष निर्धारित थी।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह गणना 2019 संशोधन से पूर्व लागू पॉक्सो कानून के संदर्भ में की गई है, जिसमें न्यूनतम सजा सात वर्ष थी।
इसी पृष्ठभूमि में अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लेख करते हुए कहा कि जब किसी व्यक्ति की आपराधिक अपील लंबित हो और उसका अंतिम निपटारा निकट भविष्य में संभावित न हो, तो उसे अनिश्चित काल तक कारावास में रखना स्वयं एक संवैधानिक प्रश्न बन जाता है।
उच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि सजा निलंबन का अर्थ दोषमुक्ति नहीं है। यह केवल अंतिम निर्णय तक की एक अंतरिम न्यायिक व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना है।
पीड़िता की सुरक्षा और सामाजिक असंतोष
पीड़िता की सुरक्षा के प्रश्न पर उच्च अदालत ने स्वीकार किया कि खतरे की आशंका वास्तविक है। इसी कारण पुलिस और प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था की व्यक्तिगत निगरानी के निर्देश दिए गए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सुरक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी है।
फिर भी, यही वह बिंदु है जहां समाज में सबसे अधिक असंतोष दिखाई देता है। पीड़िता के लिए खतरा कोई कानूनी शब्द नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सच्चाई है।
जब अदालत यह कहती है कि केवल खतरे की आशंका के आधार पर किसी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता, तो यह बात कानून की दृष्टि से सही होते हुए भी पीड़िता की पीड़ा को कम नहीं करती।
CBI की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दाखिल करते हुए यह तर्क रखा कि सजा निलंबन का यह आदेश आजीवन कारावास जैसी गंभीर सजा के प्रभाव को कमजोर करता है और मामले की प्रकृति को देखते हुए इससे सार्वजनिक विश्वास पर प्रतिकूल असर पड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CBI की ओर से यह दलील विशेष रूप से रखी गई कि पॉक्सो अधिनियम की संरचना केवल “लोक सेवक” की तकनीकी परिभाषा पर आधारित नहीं है, बल्कि उस स्थिति पर केंद्रित है जिसमें आरोपी पीड़ित बच्चे पर दबदबे या प्रभावशाली स्थिति में होता है। CBI का कहना था कि पॉक्सो कानून का उद्देश्य बच्चों को सत्ता, प्रभाव और भय के दुरुपयोग से बचाना है, और ऐसे में आरोपी की सामाजिक-राजनीतिक स्थिति को केवल IPC की संकीर्ण परिभाषा तक सीमित कर नहीं देखा जा सकता।
CBI ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह भी स्पष्ट किया कि पॉक्सो कानून में बाद के वर्षों में जो संशोधन किए गए, उनका उद्देश्य किसी नए अपराध को परिभाषित करना नहीं था। इन संशोधनों के जरिए पहले से मौजूद अपराधों के लिए केवल सजा की गंभीरता बढ़ाई गई थी, ताकि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर कानून और अधिक सख्त हो सके।
CBI का तर्क था कि ऐसे संशोधनों का प्रयोग करना संविधान के अनुच्छेद 20 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह प्रावधान केवल नए अपराधों को पीछे की तारीख से लागू करने पर रोक लगाता है, न कि पहले से अपराध माने जा चुके कृत्यों के लिए सजा को कठोर बनाने पर।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने भी इस व्याख्या को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की कि यदि विधायक या सांसद को पॉक्सो के संदर्भ में ‘लोक सेवक’ की परिधि से बाहर रखा जाता है, तो यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि एक कांस्टेबल या पटवारी तो लोक सेवक माना जाए, लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं। अदालत ने संकेत दिया कि इस प्रश्न पर विस्तृत विचार आवश्यक है।
पीठ ने यह भी दर्ज किया कि आरोपी पहले से ही पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े एक अन्य मामले में दोषसिद्ध है और उस सजा के तहत हिरासत में है। इन्हीं विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के संचालन पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया और सेंगर को अगली सुनवाई तक जेल से रिहा न किए जाने का निर्देश दिया।
साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पीड़िता को इस मामले में अलग से SLP दायर करने का वैधानिक अधिकार है और आवश्यकता पड़ने पर उसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जा सकती है।
न्याय का सवाल, जो अब टाला नहीं जा सकता
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर उस असहज सच्चाई को सामने ला दिया है, जिसे न अदालतें पूरी तरह नकार पाती हैं और न समाज अनदेखा कर सकता है। यहाँ प्रश्न किसी एक आदेश, किसी एक न्यायाधीश या किसी एक आरोपी तक सीमित नहीं है। प्रश्न उस व्यवस्था का है, जहाँ न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि हर अंतरिम फैसला अपने-आप में एक नई सामाजिक और नैतिक बहस को जन्म देने लगता है।
जब एक ओर कानून यह कहता है कि दोषसिद्धि पर अंतिम निर्णय अभी शेष है, और दूसरी ओर समाज यह देखता है कि वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रही पीड़िता को हर नए आदेश के साथ असुरक्षा का नया कारण मिल जाता है, तब टकराव अदालत और समाज के बीच नहीं, बल्कि न्याय की गति और उसकी अनुभूति के बीच होता है।
अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है और स्वयं सर्वोच्च न्यायालय यह विचार कर रहा है कि पॉक्सो जैसे कानून की व्याख्या केवल तकनीकी परिभाषाओं तक सीमित रहनी चाहिए या उसके उद्देश्य और सामाजिक प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए, तब प्रश्न और गहरा हो जाता है। यह केवल सजा निलंबन का प्रश्न नहीं रह जाता, बल्कि यह उस न्यायिक दृष्टिकोण की परीक्षा बन जाता है, जिसमें सत्ता, प्रभाव और बच्चों की सुरक्षा के बीच संतुलन साधा जाना है।
यहीं से वह सवाल सामने आता है, जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। जब न्याय की प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है और हर अंतरिम आदेश पीड़िता के मन में नई आशंकाएँ पैदा करता है, तो क्या यह बोझ केवल पीड़िता को ही उठाना चाहिए? या फिर यह जिम्मेदारी न्यायिक व्यवस्था की होनी चाहिए कि वह न्याय के साथ-साथ सुरक्षा और भरोसे का एहसास भी बनाए रखे?
शायद यही वह बिंदु है, जहाँ न्याय को सिर्फ अदालत में दिए गए आदेशों से नहीं, बल्कि इस कसौटी पर भी परखा जाना चाहिए कि व्यवस्था अपने सबसे कमजोर नागरिक के प्रति कितनी संवेदनशील और उत्तरदायी है।